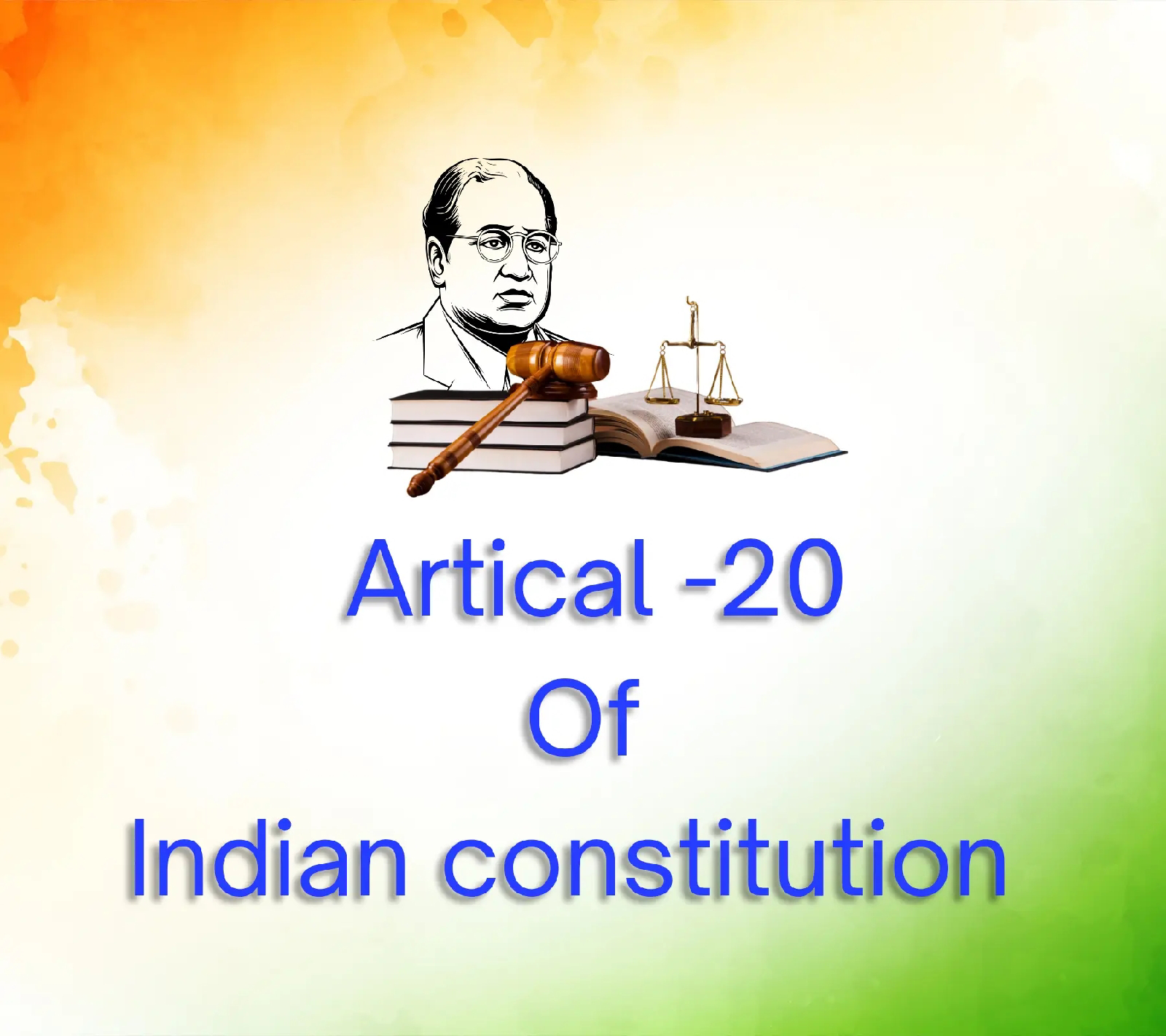मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य: भारतीय संविधान की ताकत | Fundamental Rights & Duties in Indian Constitution

संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य: एक विस्तृत विश्लेषण भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और प्रगतिशील संविधान माना जाता है। इसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की विशेष व्यवस्था की गई है। ये अधिकार और कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुरक्षित करने और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं। इस लेख में, हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मौलिक अधिकार: नागरिकों की सुरक्षा की ढाल भारतीय संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12-35) में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। आइए, इन्हें विस्तार से समझते हैं: 1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) अनुच्छेद 14 : कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 : धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 : रोजगार के अवसरों में समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का अंत करता है और इसे अपराध घोषि...